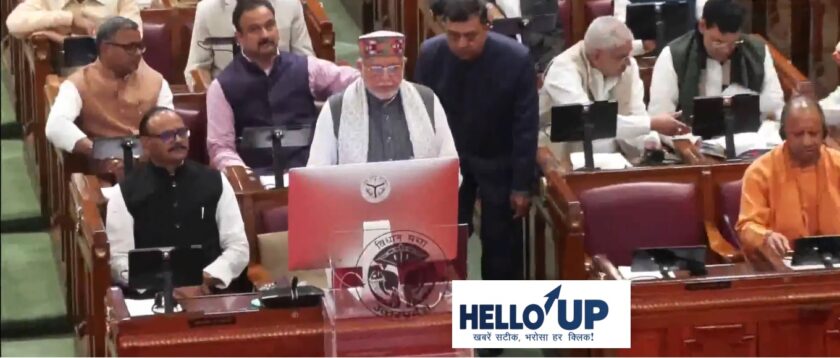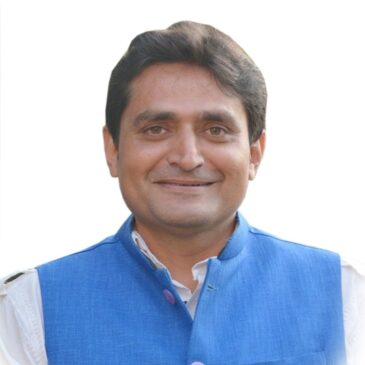
मुझे ये अच्छे से याद है कि एक समय था जब भारतीय राजनीति में संवाद की एक गरिमा हुआ करती थी। न्यूज़ चैनल की डिबेट में चाहे जितनी भी तीखी बहस हो, भाषा की मर्यादा और विचारों की शालीनता बनी रहती थी। कांग्रेस ने जहाँ देश में पहली बार आनंद शर्मा को प्रवक्ता बनाया वहीँ बीजेपी ने सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन को जबकि सीताराम येचुरी को सीपीआई ने प्रवक्ता बना पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी ये नेता न सिर्फ अपने विचारों की स्पष्टता के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी वाणी में भी संस्कार झलकता था। ये पहली बार था कि किसी राजनैतिक दल ने नेताओं को प्रवक्ता बनाया हो। आज के दौर में, वही डिबेट कटुता और व्यक्तिगत हमलों का केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां प्रवक्ता भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर अपने दल के बचाव या विपक्ष पर आक्रमण करते हैं।
हिंदू-मुस्लिम ध्यान दें : क्या उर्दू विदेशी है? सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी वर्षों पुरानी ग़लतफहमी
आप सुषमा स्वराज को याद कीजिए — एक ओजस्वी वक्ता, जो दृढ़ता से अपनी बात कहती थीं पर कभी भी शिष्टाचार की सीमा नहीं लांघती थीं। प्रमोद महाजन अपनी बातों को चुटीले अंदाज़ में रखने के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका व्यंग्य भी मर्यादित होता था। आनंद शर्मा जैसे कांग्रेसी नेता विपक्ष की आलोचना करते समय भी तथ्यों का सहारा लेते थे, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों का। सीताराम येचुरी अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते रहे, येचुरी डिबेट में जब शामिल होते तो उससे पहले किताबों के साथ होम वर्क करते थे।
उन दिनों टीवी डिबेट्स, चाहे कितनी भी गर्मजोशी से भरी हों, एक विचारोत्तेजक संवाद का रूप लेती थीं। मुद्दों पर बहस होती थी, आरोप-प्रत्यारोप होते थे, पर भाषा के स्तर को लेकर एक असामान्य सजगता थी।
वर्तमान दौर: भाषा की गिरती गरिमा
आज जब हम न्यूज़ चैनलों पर प्रवक्ताओं को सुनते हैं, तो लगता है जैसे विचारों की जगह नारेबाज़ी और तथ्यों की जगह भावनात्मक उन्माद ने ले ली है। कई बार तो प्रवक्ताओं की भाषा इतनी आक्रामक होती है कि वह लोकतांत्रिक संवाद की आत्मा को आहत कर देती है।
मैंने जो देखा है, इस गिरावट का एक बड़ा कारण है – मीडिया, विशेषकर न्यूज़ एंकरों की भूमिका। डिबेट्स को ‘TRP शो’ में बदल देने की होड़ में, एंकर बहस को मुद्दे से भटका कर एक ‘तमाशा’ बना देते हैं। आप टीवी पर देख सकते हैं, प्रवक्ताओं को उकसाने की शैली, चीख-चीख कर सवाल पूछना और बीच में ही बोलने से रोकना — ये सब संवाद नहीं, शोर को जन्म देते है।
मीडिया की भूमिका: आग में घी डालना
न्यूज़ एंकर अब शो के ‘डायरेक्टर’ के रूप में हैं, जो बहस को नाटकीय बनाने में लगे रहते हैं। इससे प्रवक्ताओं को भी यह संदेश मिलता है कि यदि वे भी उग्र भाषा और आरोपों का सहारा नहीं लेंगे, तो उनका ‘स्क्रीन टाइम’ घट जाएगा।
रॉबर्ट वाड्रा एंड कंपनी स्पेशल एडिशन: ईडी की ‘ज़मीनी मोहब्बत’ वापस ऑन स्क्रीन!
इस गिरावट के परिणाम
-
जनता में भ्रम – तथ्य और भावनात्मक उत्तेजना के बीच फर्क मिट जाता है।

-
राजनीतिक संवाद का अवमूल्यन – युवा पीढ़ी गलत उदाहरणों से सीखती है।
-
लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं – संवाद नहीं, टकराव प्रमुख हो जाता है।
समाधान क्या है?
-
प्रवक्ताओं के लिए ट्रेनिंग – भाषा की मर्यादा और तथ्यात्मक संवाद के लिए।
-
मीडिया रेगुलेशन – एंकरों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए।
-
जन जागरूकता – दर्शकों को TRP के खेल को समझना होगा और जिम्मेदार पत्रकारिता की मांग करनी होगी। क्योंकि टीवी पर वही सब नज़र आ रहा है जो जनता पसंद कर रही है।
ये भी देखें :https://www.youtube.com/watch?v=Xr60lflTd84&feature=youtu.be
मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति को फिर से एक ऐसे दौर की ओर लौटने की ज़रूरत है जहां विचारों का आदान-प्रदान गरिमामयी ढंग से हो। प्रवक्ताओं को यह समझना होगा कि वे सिर्फ किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। और मीडिया को यह याद रखना होगा कि वह चौथा स्तंभ तभी कहलाएगा जब वह निष्पक्षता और शालीनता के मूल्यों पर कायम रहेगा।